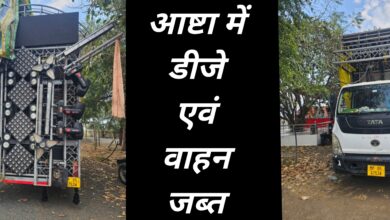संसद का मानसून सत्र : हंगामे बनाम संवाद का भविष्य
प्रशांत चौबे, लखनऊ
(संस्कृतिकर्मी एवं संस्थापक निदेशक,
अदम्य ग्लोबल फाउंडेशन)
भारतीय लोकतंत्र की आत्मा उस महान भवन में बसती है जिसे हम संसद कहते हैं। यहीं देश की नीतियाँ बनती हैं, कानून आकार लेते हैं और जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की समस्याओं को राष्ट्रीय विमर्श में बदलते हैं। परंतु यह विडंबना नहीं तो और क्या है कि जिस मंच पर विचारों की भिड़ंत से समाधान का सूर्योदय होना था, वहां अब केवल शोर, नारे और हंगामा सुनाई देता है? संसद का मानसून सत्र, जो देश की लोकतांत्रिक चेतना को पुष्ट करने का अवसर बन सकता था, बार-बार बाधित होता रहा। यह घटनाक्रम न केवल सरकार और विपक्ष के बीच संवादहीनता का संकेत है, बल्कि संसद जैसी सर्वोच्च संस्था की गरिमा के क्षरण का भी द्योतक है।
विगत कुछ वर्षों में संसद की कार्यप्रणाली पर आंकड़े ही नहीं, आम जनमानस की चिंता भी यह दर्शाने लगी है कि लोकतंत्र का यह मंदिर राजनीतिक युद्धभूमि बनता जा रहा है। मानसून सत्र 2025 कोई अपवाद नहीं रहा। टीवी चैनलों और अखबारों की सुर्खियाँ बताती हैं कि इस बार भी विधायी कार्यों की बजाय हंगामे, स्थगन, निलंबन और आरोप-प्रत्यारोप का ही बोलबाला रहा। प्रश्न यह है कि क्या संसद का मंच केवल राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बनकर रह जाएगा? क्या संवाद की संस्कृति, जो लोकतंत्र की धुरी है, अब इतिहास की बात बनती जा रही है?
भारतीय संसद का इतिहास गौरवशाली रहा है। स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक दशकों में पंडित नेहरू, डॉ. अम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेताओं ने संसद को वैचारिक मंथन का केंद्र बनाया। पक्ष और विपक्ष दोनों की बहसें शालीनता, तर्क और तथ्य पर आधारित होती थीं। लेकिन आज की स्थिति में विरोध का तरीका बदल चुका है। विपक्ष बहस की बजाय वेल में आकर प्रदर्शन करता है और सरकार बहस से बचते हुए विधेयकों को बिना चर्चा के पारित करवाने में रुचि दिखाती है। इससे दोनों पक्षों की जवाबदेही पर प्रश्नचिह्न खड़ा होता है।
मानसून सत्र के दौरान सरकार द्वारा लाए गए कई महत्त्वपूर्ण विधेयक—जैसे डेटा संरक्षण कानून, जनसंख्या नीति का प्रारूप, तीन तलाक से संबंधित संशोधन या चुनाव सुधार—पर पर्याप्त बहस नहीं हो सकी। विपक्ष की रणनीति रही कि सरकार को बिना जवाबदेही के विधेयक पारित न करने दिए जाएं, लेकिन इसका तरीका केवल हंगामा था, कोई वैकल्पिक प्रस्ताव या ठोस सुझाव नहीं। दूसरी ओर, सरकार ने यह कह कर बहस से बचने की कोशिश की कि विपक्ष संसद चलने नहीं दे रहा। यह ‘एक और एक ग्यारह’ का लोकतांत्रिक समीकरण नहीं, बल्कि ‘दोनों गलत’ की स्थिति बनाता है।
जब संसद में कामकाज नहीं होता, तो असल में नुकसान किसका होता है? जवाब है—जनता का। एक आम नागरिक संसद में अपने प्रतिनिधियों को भेजता है ताकि वे उसकी आवाज बनें, उसकी समस्याएं रखें, नीतियों पर चर्चा करें और जवाबदेही तय करें। लेकिन जब सत्र स्थगन और हंगामे में बीतता है, तो किसान की फसल, बेरोजगार का भविष्य, महिला की सुरक्षा, छात्र की शिक्षा—ये सब मुद्दे पीछे छूट जाते हैं।
2025 के मानसून सत्र में रोजगार, महंगाई, महिला आरक्षण, चिकित्सा व्यवस्था और जलवायु परिवर्तन जैसे ज्वलंत विषयों पर सार्थक चर्चा नहीं हो सकी। यदि विपक्ष वेल में प्रदर्शन करता रहा और सत्ता पक्ष जवाब देने की बजाय मौन रहा या विधेयकों को ध्वनि मत से पारित करवा देता रहा, तो यह पारदर्शिता और जवाबदेही के लोकतांत्रिक सिद्धांतों का अपमान है।
यह भी महत्वपूर्ण है कि संसद का मंच अब रणनीति और इवेंट मैनेजमेंट का स्थान बनता जा रहा है। विपक्ष जानबूझ कर हंगामा करता है ताकि सरकार को कठघरे में खड़ा किया जा सके, वहीं सरकार सत्र की शुरुआत से ही ‘काम नहीं करने देने वाले विपक्ष’ की छवि बनाकर सहानुभूति अर्जित करती है। यह एक तरह का जन-
-धोखा है, जिसमें दोनों पक्ष अपनी राजनीति साध रहे हैं और लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य—जनसेवा—कहीं गुम होता जा रहा है।
इस मानसून सत्र में सांसदों के निलंबन की घटनाएं, कई महत्वपूर्ण विधेयकों को बिना चर्चा पारित कर देना और प्रधानमंत्री का विपक्ष की चिंताओं को ‘बेहूदी राजनीति’ कहकर खारिज कर देना—इन सबने यह प्रश्न खड़ा किया है कि क्या हम संवाद के युग से वाकयुद्ध के युग में प्रवेश कर चुके हैं?
इस प्रश्न का उत्तर केवल आलोचना से नहीं, बल्कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण से ढूंढ़ा जाना चाहिए कि संसद की गरिमा को कैसे बहाल किया जा सकता है? प्रथम आवश्यकता है—राजनीतिक इच्छाशक्ति की। जब तक सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस बात को नहीं स्वीकार करेंगे कि संसद का मूल कार्य बहस और संवाद है, तब तक सुधार की कोई भी कोशिश सतही ही सिद्ध होगी। सरकार को चाहिए कि वह विपक्ष की आलोचनाओं को केवल राजनीति कह कर न टाले, बल्कि उन्हें सुनने, समझने और उत्तर देने की संस्कृति विकसित करे। वहीं विपक्ष को भी यह समझना होगा कि वेल में आकर नारे लगाने और आसन के पास प्रदर्शन करने से कोई लोकतांत्रिक उद्देश्य सिद्ध नहीं होता। जनता ने विपक्ष को नकारात्मक राजनीति के लिए नहीं, बल्कि सशक्त विकल्प और जनहित में प्रश्न उठाने के लिए संसद में भेजा है।
भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में जहां विविधता इतनी व्यापक है कि एक कानून का असर हर क्षेत्र में भिन्न हो सकता है, वहां परिपक्व, बहुआयामी और विवेकपूर्ण बहस