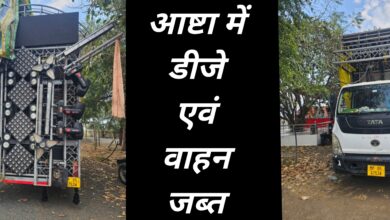‘डिजिटल इंडिया’ से ‘डिजिटल असमानता’ तक : क्या सबको मिल रहा है बराबरी का लाभ?
डॉ. शैलेश शुक्ला, लखनऊ
(वरिष्ठ लेखक, पत्रकार, साहित्यकार)
जब 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘डिजिटल इंडिया’ का उद्घोष किया था, तब देश ने उम्मीद की थी कि तकनीक के इस अभियान से गाँव-गाँव, जन-जन तक समान अवसर पहुंचेगा। यह एक ऐसा सपना था जिसमें एक किसान, एक छात्रा, एक मजदूर, एक शिक्षक और एक बुजुर्ग—all would be equally empowered through a digital ecosystem. लेकिन आज, एक दशक के करीब खड़े होकर यदि हम पीछे मुड़कर देखें, तो तस्वीर उतनी उजली नहीं दिखती जितनी प्रचारित की गई। डिजिटल इंडिया की रोशनी भले ही महानगरों में दमक रही हो, लेकिन उसी रोशनी की छाया में भारत का एक बड़ा हिस्सा डिजिटल अंधकार में डूबा हुआ है। सवाल यह नहीं है कि भारत डिजिटल हो रहा है या नहीं; सवाल यह है कि यह परिवर्तन सबको समान रूप से सशक्त बना रहा है या कुछ को और अधिक शक्तिशाली तथा अन्य को और भी वंचित?
डिजिटल इंडिया का मूल उद्देश्य था – नागरिक सेवाओं की डिजिटल पहुंच, डिजिटली साक्षर समाज का निर्माण, इंटरनेट के माध्यम से शासन की पारदर्शिता और रोजगार के नए अवसरों का सृजन। इसमें भारतनेट परियोजना, डिजिटल लॉकर, उमंग ऐप, डिजीलॉकर, डिजिटल भुगतान, आधार आधारित सेवाएँ और ग्रामीण क्षेत्रों में CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) जैसे उपायों को बल मिला। भारत आज विश्व के सबसे बड़े डेटा उपभोक्ताओं में है। UPI ट्रांजैक्शन की संख्या प्रतिदिन करोड़ों में है। सरकारी सेवाओं की ऑनलाइन उपलब्धता भी बढ़ी है। लेकिन इन आँकड़ों के पीछे जो असली कहानी छुपी है, वह है ‘डिजिटल डिवाइड’ यानी ‘डिजिटल असमानता’ की।
नेशनल सैंपल सर्वे (NSSO) के आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण भारत में मात्र 15% परिवारों के पास ही इंटरनेट की सुविधा है। इसके विपरीत शहरी क्षेत्रों में यह संख्या 42% तक जाती है। लेकिन इंटरनेट सुविधा केवल मौजूद होना ही पर्याप्त नहीं; सवाल यह भी है कि क्या उपयोगकर्ता के पास आवश्यक डिवाइस, डिजिटल साक्षरता और आर्थिक सामर्थ्य है कि वह उस सुविधा का सही उपयोग कर सके? 2021 में ऑक्सफैम इंडिया की एक रिपोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि केवल 8% ग्रामीण भारतीय ही डिजिटल सेवाओं का सुचारु उपयोग कर पाते हैं।
कोविड-19 महामारी के दौरान जब शिक्षण पूरी तरह से ऑनलाइन हो गया, तब ‘डिजिटल इंडिया’ के स्वप्न का कड़वा यथार्थ सामने आया। देश के लाखों छात्र ऐसे थे जो स्मार्टफोन, लैपटॉप या इंटरनेट की अनुपलब्धता के कारण शिक्षा से वंचित रह गए। एक तरफ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे शहरों में छात्र हाई-स्पीड इंटरनेट के साथ वर्चुअल क्लासेज़ से जुड़े रहे, वहीं दूसरी तरफ बिहार, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में विद्यार्थी रेडियो या ब्लैकबोर्ड तक सीमित रह गए। कई मामलों में एक ही घर में दो या तीन बच्चों को एक ही मोबाइल से पढ़ाई करनी पड़ी। क्या इसे हम ‘डिजिटल समावेशीकरण’ कहेंगे या ‘डिजिटल बहिष्करण’?
डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने रोजगार और व्यवसाय के नए आयाम खोल दिए हैं—फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन मार्केटप्लेस, डिजिटल कंटेंट, ऐप्स और सोशल मीडिया आधारित आय। लेकिन ये अवसर केवल उन्हीं के लिए सुलभ हैं जिनके पास इंटरनेट की गति, डिवाइस की सुविधा और डिजिटल कौशल है। देश की बड़ी जनसंख्या अब भी पारंपरिक रोजगारों और श्रम आधारित कार्यों पर निर्भर है। जब मनरेगा जैसी योजनाएँ भी ‘एप आधारित उपस्थिति’ पर केंद्रित हो जाती हैं, तब एक अशिक्षित मज़दूर या तकनीकी जानकारी से वंचित महिला कैसे अपने अधिकारों को हासिल कर पाएगी? सरकार के डिजिटल पोर्टल्स का जाल अगर स्थानीय भाषा, तकनीकी सहायता और यूज़र फ्रेंडली सिस्टम के अभाव में है, तो यह सुविधा नहीं, बल्कि बाधा बन जाती है।
डिजिटल इंडिया का एक और अंधकारमय पहलू है—भाषायी और वर्गीय असमानता। भारत में अधिकांश डिजिटल सामग्री अंग्रेज़ी और कुछ चुनिंदा भारतीय भाषाओं तक ही सीमित है। हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी प्रशासनिक ऐप्स अंग्रेज़ी-प्रधान हैं, जिससे स्थानीय उपयोगकर्ताओं को कठिनाई होती है। डिजिटल असमानता केवल इंटरनेट की अनुपलब्धता तक सीमित नहीं, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और वर्ग आधारित समस्या भी बन चुकी है। एक ओर तकनीकी कंपनियों के पास बहुभाषीय सॉफ्टवेयर की क्षमता है, दूसरी ओर सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन भाषा और डिजिटल समावेशन को दरकिनार करता नजर आता है।
सरकार ने डिजिटल समावेशन (Digital Inclusion) को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं—जैसे ‘प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान’ (PMGDISHA), ‘भारतनेट’ के तहत गाँवों में फाइबर नेटवर्क बिछाने का कार्य, CSC के माध्यम से ग्राम स्तरीय सेवाएं प्रदान करने का प्रयास और युवाओं के लिए कोडिंग-प्रशिक्षण की पहलें। इन योजनाओं का उद्देश्य हर नागरिक तक तकनीक की पहुँच और उसका न्यायसंगत लाभ पहुंचाना रहा है। लेकिन ये प्रयास अक्सर भ्रष्टाचार, अव्यवस्था, स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण की कमी और संसाधनों की असमान उपलब्धता के कारण विफल होते रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, कई गाँवों में CSC सेंटर केवल कागज़ों पर ही संचालित हैं, या उन्हें प्रभावी प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता नहीं मिलती, जिससे वे जनता तक सेवाएं पहुंचाने में अक्षम हो जाते हैं।
दूसरी ओर, भारतनेट की परियोजना कई बार समयसीमा से पीछे रह गई है। वर्ष 2023 के अंत तक देश के सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित था, लेकिन सरकार की ही रिपोर्ट के अनुसार 50% से कम पंचायतें पूरी तरह कनेक्ट हो सकीं। कहीं तकनीकी बाधाएं थीं, कहीं ठेकेदारों की उदासीनता, तो कहीं बड़ी लापरवाही।